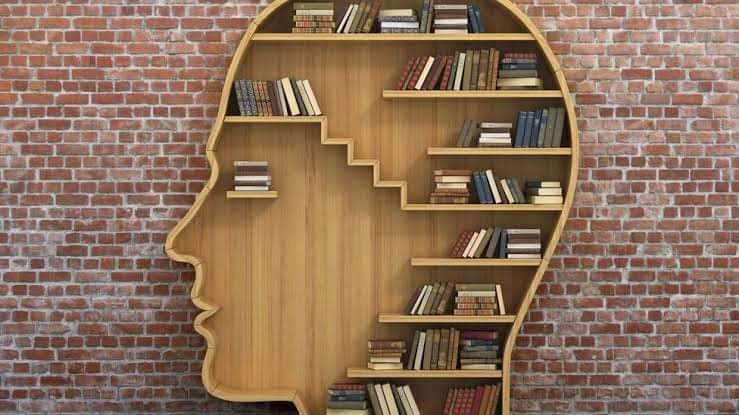क्या विदेशी विश्वविद्यालय देश के लिए हानिकारक हैं?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने देने के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय शिक्षा इधर कुआ, उधर खाई और बीच में गड्ढा वाली तीन-तरफा बदहाली में फंसी हुई है। एक तरफ स्तर के लिहाज से मामूली उच्च-शिक्षा देने वाले करीब एक हजार विश्वविद्यालयों और 42 हजार कॉलेजों से साल-दर-साल निकल रही बीए-एमए-पीएचडी डिग्रीधारी भीड़ है।
बाजार में इसका एक बड़ा हिस्सा साधारण नौकरी पाने के काबिल भी नहीं माना जाता। यानी इसकी ‘एम्प्लॉयबिलिटी’ नगण्य है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा तक समाज के पांच से दस फीसदी अमीर तबके की ही पहुंच है। अब इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा भी जुड़ जाएगी।
सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित समझे जाने वाले डीयू में अगर किसी छात्र को तीन साल के ग्रेजुएट कोर्स की खातिर पचास हजार रुपए तक देना पड़ते हैं तो निजी क्षेत्र के अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले धनी छात्रों को चार साल के कोर्स के लिए पच्चीस से तीस लाख रुपए का भुगतान करना होता है। कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड में दाखिले के लिए कितनी फीस देनी होगी, अंदाजा लगा लीजिए।
इस कुए और खाई के बीच के गड्ढों में धंसी हुई हमारी शिक्षा-व्यवस्था पर सरकारी जुमलेबाजी ने विश्व-गुरु बनने का दायित्व डाल रखा है। जाहिर है कि विश्व-बाजार में मलाईदार नौकरियां करने वाले गिने-चुने भारतीयों की नयी पीढ़ियां निजी और विदेशी परिसरों से निकलेंगी।
सस्ते श्रम के रूप में उनकी खिदमत करने वाले ‘शिक्षित’ असंख्य भारतीयों की पीढ़ियां ऐसे विश्वविद्यालयों से निकलेंगी, जिन्हें सौ-सवा सौ साल पहले भारतीय शिक्षा के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों के नाम पर स्थापित किया गया था। नई शिक्षा नीति के मुताबिक लिए गए इस फैसले के पक्ष में दी जा रही दलीलें मुख्य रूप से आर्थिक हैं।
जैसे 2024 तक 18 लाख भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आठ अरब डॉलर खर्च करने वाले हैं, उनका तीन-चौथाई हिस्सा बचाया जा सकेगा। इससे प्रतिभा पलायन भी रुक सकता है। सर्वाधिक हास्यास्पद तर्क यह है कि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय विदेशियों से प्रतियोगिता करके अपना स्तर सुधार सकेंगे।
हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली की मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि किसी जमाने में अकादमिक चमक रखने वाली ये संस्थाएं अब केवल प्रशासनिक इकाइयां बनकर रह गई हैं। कहना न होगा कि विश्वविद्यालय जैसी बड़ी संस्था चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है, जो एक अकादमिक ढांचे की सेवा करता है।
आजकल यह अकादमिक ढांचा उत्साहहीन अध्यापन और डिग्रियां बांटने तक सिमटकर रह गया है। इस पतित स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है पीएचडी या शोध-प्रबंध का गिरता स्तर। ऐसे शोध-प्रबंध दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिनमें कोई नया निष्कर्ष निकाला गया हो।
दरअसल, प्रबंध अंग्रेजी में लिखा गया हो या किसी भारतीय भाषा में- उसका पंजीकरण, उसके लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति, उसके लिए होने वाला फील्डवर्क और अंत में उसे लिखे जाने के बाद उसकी जांच की प्रक्रिया में अकादमिक ईमानदारी, प्रतिभा और ज्ञान से चमकते हुए श्रम की भूमिका न के बराबर होती है।
ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं कि समाज-विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी करने वाले शोधार्थी को गणित या भौतिकी का प्रोफेसर ‘गाइड’ कर रहा हो। अगर कहीं कोई प्रतिभा बची हुई भी है तो वह शिक्षकों की नौकरियों की बंदरबांट होते समय कुम्हला जाती है। प्रवक्ता पद पर एक-एक नौकरी के लिए ऐसी-ऐसी राजनीतिक तिकड़में लगाई जाती हैं कि पढ़ने-लिखने वाले उम्मीदवार तक उनकी पहुंच असम्भव साबित होती है।
इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि करीब डेढ़-दो सौ साल तक पश्चिमी विश्वविद्यालयों की नकल करने की हमारी कोशिश अब घोषित रूप से नाकाम हो गई है। जो हमारे आदर्श थे, वे अब हमारा मुंह चिढ़ाते हुए हमारे जेएनयू, बीएचयू, एएमयू या डीयू की बगल में अपना परिसर खोलेंगे।
डॉलरों, पाउंडों और यूरो के रूप में मुनाफा कमाकर ये विदेशी विश्वविद्यालय फेमा कानून की शर्तों का पालन करते हुए अपने देश ले जाएंगे। और उनकी बेहतर कार्बन कॉपी बनने का दम भरने वाले खुद को निचले पायदान पर पाएंगे।
एक हजार विश्वविद्यालयों और 42 हजार कॉलेजों से साल-दर-साल निकल रही बीए-एमए-पीएचडी डिग्रीधारी भीड़ है। बाजार में इसका बड़ा हिस्सा साधारण नौकरी के काबिल भी नहीं माना जाता।
- यह भी पढ़े………..
- पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं प्रवासी भारतीय,कैसे?
- क्या जनगणना की जिम्मेदारी पूरी करना आवश्यक है?
- सर्दी के मौसम में बच्चों में संक्रमण की प्रबल संभावना