क्या होती है खेतों की चकबंदी?
पंजाब में सबसे पहले 1920 में चकबंदी हुई थी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
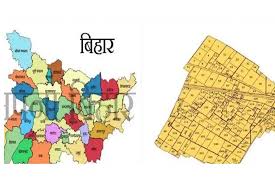
बिहार में 70 के दशक में चकबंदी की शुरुआत हुई थी. 1992 में इसे बंद कर दिया गया. हालांकि, 2021 में फिर एक बार इसे चालू कर दिया गया. इस बार कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया. विदेशों में जहां खेती की जाती है, वहां अमूमन एक साथ काफी बड़े खेत होते हैं. इससे कुछ भी उगाने की लागत कम हो जाती है. खेती के लिए आधुनिक व बड़े उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत में अधिकांश राज्यों में ऐसा नहीं होता है. इसलिए सरकार ने चकबंदी की शुरुआत की है.
चकबंदी का मतलब है इकट्ठा कर देना. खेती के संदर्भ में देखें तो अलग-अलग जगह टुकड़ों में पड़ी आपकी जमीन को एक जगह ले आना. उदाहरण के लिए किसान A के पास गांव में 3 अलग-अलग जगहों पर खेत हैं. उसे तीन जगह मैनेज करना पड़ेगा. परंतु यदि चकबंदी होती है तो जमीन के सभी मालिकों में बंटवारा कुछ तरीके से होगा कि सभी को उनके खेत एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाएं.
किसान A को 3 टुकड़ों के बराबर एक जगह जमीन मिल जाएगी. बता दें कि परिवारों के बंटवारे के कारण पहले बड़े रहे खेत समय के साथ छोटे होते जाते हैं. इन खेतों में मेहनत और खर्च तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है, लेकिन फसल और उससे होने वाली कमाई ज्यादा नहीं होती. वहीं, अगर एक ही जगह खेत हों तो लागत कम हो सकती है और किसान को ज्यादा लाभ मिल सकता है.
चकबंदी कानून का इतिहास
भारत में चकबंदी कानून की शुरुआत सबसे पहले पंजाब प्रान्त में एक प्रयोग के रूप में हुई, और वो साल था सन् 1920, यानि ये आज़ादी से पहले की बात है। इस समय देश में अंग्रेज़ों का शासन चलता था। उस समय अंग्रेजी सरकार ने सभी नियम अपने फायदे को ध्यान में रखकर बनाए थे।
जब चकबंदी के इस प्रयोग को सफलता मिली, तो इसे सन् 1936 में कानूनी तौर पर लागू करने का विचार बनाया। इससे पंजाब में तो कुछ हद तक सफलता मिली, परंतु बाकी राज्यों ने चकबंदी को लेकर कुछ ख़ास रुझान नहीं दिखाया।
स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने चकबंदी के नियमों में कुछ सशोधन किए। बदलाव के बाद बंबई में सन 1947 में पारित नियम में ऐलान किया गया कि जहां उचित हो वहां चकबंदी की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। घोषणा होने के बाद इस नियम को कुछ प्रदेशों में लागू भी किया गया।
इन प्रदेशों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, बिहार और हैदराबाद शामिल थे। भारत सरकार के एक आंकड़े की मानें तो सन् 1956 तक 110.09 लाख एकड़ की ज़मीन चकबंदी क्षेत्र में आ गयी थी। वहीं वर्ष 1960 तक ये आंकड़ा बढ़कर 230 एकड़ तक हो गया।
चकबंदी का कारण
सरकार ने उपरोक्त बात को आधार बनाते हुए किसानों को एक ही जगह पर खेत देना शुरू कर दिया. जिन किसानों के पास अलग-अलग स्थानों पर छोटे खेत थे उन्हें उतनी जमीन के बराबर एक ही जगह पर खेत दे दिए गए. हर राज्य के अलग-अलग चकबंदी कानून होते हैं. चकबंदी के तहत मिले खेतों को चक कहा जाता है. कई बार सरकार 2-3 में जमीन दे देती है. हालांकि, ये चकबंदी की मूल भावना के विपरीत है.
वरदान या अभिशाप
चकबंदी को आमतौर पर किसानों के लिए अच्छा ही माना जाता है. हालांकि, इसके कुछ नुकसान या फिर यूं कहे कि जटिलताएं हैं. पहले बात इसकी अच्छाई की. चकबंदी से खेत में फसल उगाने के में होने वाला औसत खर्च घट जाता है. सरकार द्वारा कानूनी रूप से आपको खेते दिए जाने से किसी भी तरह का जमीन विवाद निपट जाता है. बड़े खेत होने से बड़े उपकरण इस्तेमाल हो सकते हैं जो फसल की जल्दी बुआई व कटाई में मदद करते हैं. हर कुछ दूर पर पगडंडियां नहीं बनानी होती, इससे जमीन बर्बाद होने से बचती है. एक ही जगह अगर खेत हों तो उसका रख-रखाव आसानी से किया जा सकता है.
चकबंदी होने से बिखरे हुए खेत एक जगह हो जाते हैं।
छोटे-छोटे खेतों की मेड़ों में भूमि बर्बाद नहीं होती है।
खेत बड़े हो जाने से मशीनीकरण आसान हो जाता है।
खेत का आकार अधिक हो जाने से लागत घट जाती है।
किसान अपने सभी खेतों की आसानी से देखभाल कर सकते हैं।
किसानों को अक्सर अपनी पैतृक जमीन छोड़नी पड़ती है, जिससे उनका लगाव होता है. अगर 2-3 चक मिल जाएं तो चकबंदी का सारा मकसद ही मिट्टी में मिल जाता है. एक बड़ी समस्या यह भी आती है कि कई बार किसानों को जो चक दिया जाता है वह उनकी अपनी जमीन से कम पैदावार वाला होता है. ऐसे में कुछ किसानों को तो अच्छी जमीन मिल जाती है लेकिन कुछ को कम उपजाऊ वाले खेतों से संतोष करना पड़ता है. इसका असर अंतत: उनकी पैदावार और कमाई पर नजर आता है.
- यह भी पढ़े……….
- क्या बिहार में चकबंदी का कोई औचित्य नहीं है?
- क्या बिहार में परिमार्जन एक विचारणीय प्रश्न बन गया है?
- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है!













